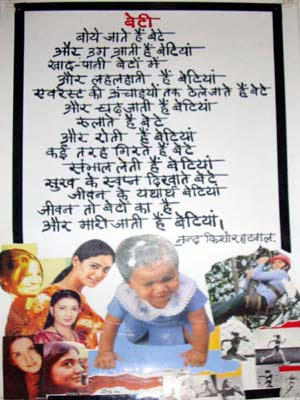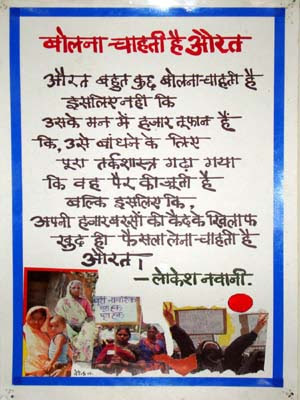पण कब तलक

मेरा बिजाल्यां बीज अंगर्ला सार-खार मेरि भम्मकली गोसी कबि मेरु भुक्कि नि जालू कोठार, दबलौं कि टुटलि टक्क पण, कब तलक मेरा जंगळूं का बाघ अपणा बोंण राला मेरा गोठ्यार का गोरु बाखरा उजाड़ जैकि गेड़ बांधी गाळी ल्याला दूद्याळ् थोरी रांभी कि पिताली ज्यू पिजण तक पण, कब तलक मेरा देशूं लखायां फिर बौडिक आला पुंगड़्यों मा मिस्यां डुट्याळ फंड्डु लौटी जाला पिठी कू बिठ्गु मुंड मा कू भारू कम ह्वै जालु कुछ हद तक पण, कब तलक Copyright@ Dhanesh Kothari Photo source- Mera pahad