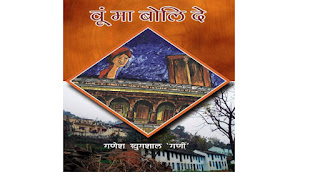राजुला-मालूशाही पहाड़ की सबसे प्रसिद्ध अमर प्रेम कहानी है। यह दो प्रेमियों के मिलन में आने वाले कष्टों , दो जातियों , दो देशों , दो अलग परिवेश में रहने वाले प्रेमियों का कथानक है। तब सामाजिक बंधनों में जकड़े समाज के सामने यह चुनौती भी थी। यहां एक तरफ बैराठ का संपन्न राजघराना रहा, वहीं दूसरी ओर एक साधारण व्यापारी परिवार। तब इन दो संस्कृतियों का मिलन आसान नहीं था। लेकिन एक प्रेमिका की चाह और प्रेमी के समर्पण ने प्रेम की ऐसी इबारत लिखी, जो तत्कालीन सामाजिक ढांचे को तोड़ते हुए नया इतिहास रच गई। राजुला मालूशाही की प्रचलित लोकगाथा कुमांऊं के पहले राजवंश कत्यूर के किसी वंशज को लेकर यह कहानी है। उस समय कत्यूरों की राजधानी बैराठ वर्तमान चौखुटिया थी। जनश्रुतियों के अनुसार बैराठ में तब राजा दोलूशाह शासन करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। इसके लिए उन्होंने कई मनौतियां मनाई। अन्त में उन्हें किसी ने बताया कि वह बागनाथ ( बागेश्वर ) में शिव की अराधना करें, तो उन्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है। वह बागनाथ के मंदिर गये। वहां उनकी मुलाकात भोट के व्यापारी सुनपत शौका और उ