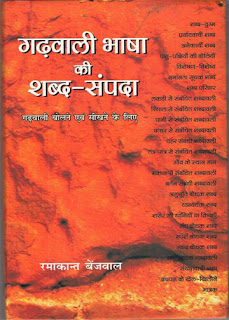लोकसभा मा क्य काम-काज हूंद भै ?
(Garhwali Satire, Garhwal Humorous essays, Satire in Uttarakahndi Languages, Himalayan Languages Satire and Humour ) अच्काल पार्लियामेंट मा रोज इथगा हंगामा/घ्याळ होंद बल लोकसभा या राज्यसभा खुल्दा नीन अर दुसर दिनों बान मुल्तबी/ 'ऐडजौर्नड फॉर द डे' करे जान्दन. बस याँ से पारिलियामेंट सदस्य बिसरी गेन, भूलिगेन की लोकसभा या राज्यसभा मा काम काज क्य हूंद ? एम् पीयूँ तैं अब पता इ नी च बल लोक सभा या राज्य सभा सदस्यों मा क्वी कम बि होंद. अब सी पर्स्या की त बात च. परसी मि अपुण एम्.पी (राज्य सभा सदस्य) दगड्या कु इख ग्यों बल मि बि ज़रा पार्लियामेंट देखूं अर उख क्य क्य होणु च वांको जायजा बि ल्हीयूँ. अब जन कि मेरो दगड्या बिना बातौ अहिंसक मनिख च वै तैं कमांडो की सेक्युरिटी त छ्वाड़ो एमपी हाउस कुणि एक चौकीदार बि नि मील. म्यार दगडया एमपी न बीस पचीस माख मारिन, दस पन्दरा मूस पकड़ीन अर पिंजरा मा बन्द कौरिन अर औथेरिटयूँ तैं बि दिखाई तबी बि मेरो दगडया तैं जेड त छ्वाड़ो ए सेक्युरिटी बि नि मील उलटां एक चौकीदार छौ वै तैं बि के हैंक नगर पालिका सेवक को इख भेजी दे. त मै तैं दगड्या एमपी क इख जाण मा क