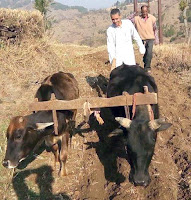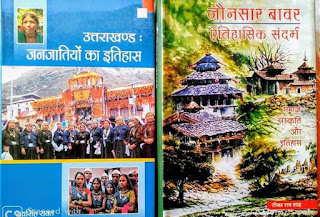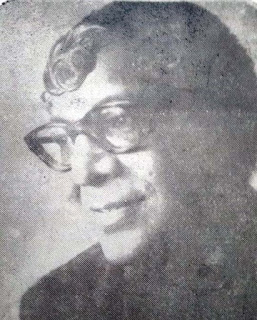आधुनिक गढ़़वाली कविता का संक्षिप्त इतिहास

भीष्म कुकरेती (मुंबई) // गढ़़वाली भाषा का प्रारम्भिक काल गढ़़वाली भाषाई इतिहास अन्वेषण हेतु कोई विशेष प्रयत्न नहीं हुए हैं। अन्वेषणीय वैज्ञानिक आधारों पर कतिपय प्रयत्न डॉ. गुणानन्द जुयाल, डॉ. गोविन्द चातक, डॉ. बिहारी लाल जालंधरी, डॉ. जयंती प्रसाद नौटियाल ने अवश्य किया किन्तु तदुपरांत पीएचडी करने के पश्चात इन सुधिजनों ने अपनी खोजों का विकास नहीं किया और इनके शोध भी थमे रह गए। डॉ. नन्दकिशोर ढौंडियाल और इनके शिष्यों के कतिपय शोध प्रशंसनीय हैं पर इनके शोध में भी क्रमता का नितांत अभाव है। चूंकि भाषा के इतिहास में क्षेत्रीय इतिहास, सामाजिक विश्लेषण, भाषा विज्ञान आदि का अथक ज्ञान और अन्वेषण आवश्यक है। अतः इस विषय पर वांछनीय अन्वेषण की अभी भी आवश्यकता है। अन्य विद्वानों में श्री बलदेव प्रसाद नौटियाल, संस्कृत विद्वान् धस्माना, भजन सिंह सिंह, अबोध बंधु बहुगुणा, मोहन लाल बाबुलकर, रमा प्रसाद घिल्डियाल 'पहाड़ी', भीष्म कुकरेती आदि के गढ़वाली भाषा का इतिहास खोज कार्य वैज्ञानिक कम भावनात्मक अधिक हैं। इन विद्वानों के कार्य में क्रमता और वैज्ञनिक सन्दर्भों का अभाव भी मिलता है। इसके अतिरि