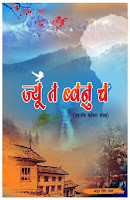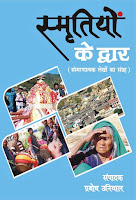अथश्री प्रयाग कथाः सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगियों पर रोचक उपन्यास

- गंभीर सिंह पालनी// प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे युवाओं को लेकर हिन्दी में लिखे गए उपन्यासों ‘डार्क हॉर्स’ (लेखकः नीलोत्पल मृणाल) तथा ‘अल्पाहारी गृहत्यागी’ (लेखकः प्रचंड प्रवीर) की सूची में हाल ही में एक और नये उपन्यास का नाम जुड़ गया है; यह उपन्यास है श्री ललित मोहन रयाल का नया उपन्यास ‘अथश्री प्रयाग कथा ’। जहां एक ओर ‘अल्पाहारी गृहत्यागी’ उपन्यास में आई.आई.टी. की प्रवेश-परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों की दुनिया का चित्रण है तो ‘डार्क हॉर्स’ उपन्यास शानो-शौकत वाली नौकरी आई.ए.एस. की अभिलाषा लिये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे ग्रेजुएट/पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं की ज़िंदगी और उनके संघर्षों को लेकर है। श्री ललित मोहन रयाल का नया उपन्यास ‘अथश्री प्रयागकथा’ भी सिविल सेवा के लिए चुने जाने हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे युवाओं की ज़िंदगी और उन के संघर्षों को लेकर है। ‘डार्क हॉर्स’ उपन्यास में जहां दिल्ली के मुखर्जी नगर व उसके आस-पास रह रहे ऐसे प्रतियोगी छात्रों की दुनिया है तो ‘अथश्री प्रयाग कथा’ में इलाहाबाद में रहकर संघर्ष कर रहे ऐसे छात्रों क