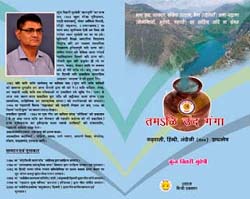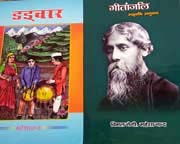इ ब्यठुला - इ जनना (गढ़वाली)

गीत (अनुवादित) / पयाश पोखड़ा // ************************* इ ब्यठुला इ जनना कै भि चीजि की खत-पत खत्ता फोळ नि करदा न बेकार करदा न बरबाद करदा बिटोळणा रंदि समळणा रंदि ढकणा रंदि बंधणा रंदि ह्वै साक जख तक आस विसवास तक कभि तुलपाणा रंदि कभि टंक्यांणा रंदि कभि घम्याणा रंदि कभि हवा बतास कभि छट्यांणा रंदि कभि बिराणा रंदि कभि त्वड़णा रंदि कभि ज्वड़णा रंदि कतगै दां अपणै घारम खालि डब्बा जमा करणा रंदि कभि कागज पत्तर कभि धोति कत्तर उलटणा पुलटणा अर गुलटणा रंदि सुबेरा की कल्यौ रोटि रुमक दां म्वड़खी बणै चपाणा रंदि खाणा रंदि अर बासी भुज्जि ठंडा तवा म गरम करणा रंदि गरम चुला दगड़ खांदा म्याळों थैं लिपणा रंदि अर लिपणा रंदि सबुथैं खवै पिवैकि तब फिर अपणि थकुलि सजैकि द्यखणा रंदि चिर्यां लारा-लत्ता टुट्यूं बटन झिल्लु बटनकाज दुबणाणा रंदि टंगणा रंदि सिलणा रंदि सूखू अचार सीला पापड़ मट्यरु लगीं दाळ सड़्यूं आरु आम कबस्यूं साग या फिर दुख दिंदरा रिस्ता बटोळणि रंदि समळणि रंदि ढकणि रंदि बंधणि र