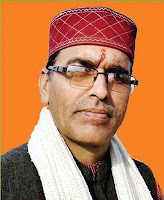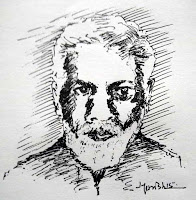अब....!
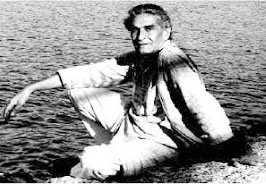
गिर्दा ! आपने कहा था हमारी हिम्मत बांधे रखने के लिए ‘जैंता इक दिन त आलो ये दिन ये दुनि में’ तब से हम भी इंतजार में हैं वो ‘दिन’ आने के हिम्मत हमने अब भी बांधी हुई है उसी एक पंक्ति के भरोसे दिन हमारे आएंगे; नहीं मालूम हाँ, उन ब्योपारियों के आ गए जिनसे तुमने पूछा था ‘बोल ब्योपारी अब क्या होगा..’ तुम्हारे चले जाने के दस साल/ और उत्तराखंड राज्य बनने के बीस साल/ बाद हमारे अंदर टूटते ‘पहाड़’ को अब कौन थामे हुए रखेगा गिर्दा! कदाचित अब हम हिम्मत को बांध कर नहीं रख सके तो कौन कहेगा फिर हमसे ‘जैंता इक दिन त आलो ये दिन ये दुनि में’ गिर्दा! चले आओ फिर से और गाओ बार बार गाओ ... धन मयेड़ी मेरो यो जनम तेरि कोखि महान, मेरा हिमाला..... • धनेश कोठारी - फोटो साभार - Google